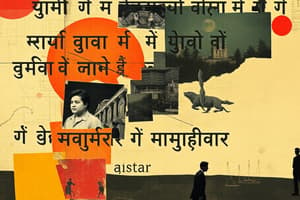Podcast
Questions and Answers
Vilken typ av sats är 'Om det regnar, stannar vi hemma'?
Vilken typ av sats är 'Om det regnar, stannar vi hemma'?
- Villkorlig sats (correct)
- Enkel sats
- Sammansatt sats
- Frågesats
Vilken av följande fraser är ett exempel på en dvandva samas (kopulativ sammansättning)?
Vilken av följande fraser är ett exempel på en dvandva samas (kopulativ sammansättning)?
- `prativarsh` (varje år)
- `din-raat` (dag och natt) (correct)
- `trylok` (tre världar)
- `rajaputra` (kungens son)
Vilket sandhi-exempel illustrerar principen att en vokal följt av en annan vokal kan resultera i en sammanslagning eller förändring av ljuden?
Vilket sandhi-exempel illustrerar principen att en vokal följt av en annan vokal kan resultera i en sammanslagning eller förändring av ljuden?
- Sammanslagningen av `tat + maya` till `tanmaya`.
- Sammanslagningen av `jagath + nath` till `jagannath`.
- Sammanslagningen av `dik + ant` till `digant`.
- Sammanslagningen av `sura + indra` till `surendra`. (correct)
Vilket alternativ korrekt illustrerar användningen av vachan (numerus) i hindi, där ett substantiv ändrar form för att indikera plural?
Vilket alternativ korrekt illustrerar användningen av vachan (numerus) i hindi, där ett substantiv ändrar form för att indikera plural?
Vilket skiljetecken används för att indikera ett kort uppehåll i en mening och används ofta för att separera element i en lista?
Vilket skiljetecken används för att indikera ett kort uppehåll i en mening och används ofta för att separera element i en lista?
Flashcards
Vaakya ke prakar (Menings typer)
Vaakya ke prakar (Menings typer)
Olika typer av meningar baserat på deras struktur och funktion.
Samas (Sammansättning)
Samas (Sammansättning)
En process där två eller flera ord slås samman för att bilda ett nytt, kortare ord.
Sandhi (Ljudförändring)
Sandhi (Ljudförändring)
Kombinationen av två ljud eller bokstäver som resulterar i en förändring i ljudet.
Vachan (Numerus)
Vachan (Numerus)
Signup and view all the flashcards
Viram Chinh (Punctuationstecken)
Viram Chinh (Punctuationstecken)
Signup and view all the flashcards
Study Notes
- व्याकरण कक्षा 7 के लिए नोट्स
वाक्य के प्रकार
- वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो एक विचार को व्यक्त करती है।
- वाक्यों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि अर्थ, रचना और प्रयोग।
- अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार:
- विधानवाचक वाक्य: ये वाक्य किसी तथ्य या जानकारी को बताते हैं। उदाहरण: "सूर्य पूर्व में उगता है।"
- निषेधवाचक वाक्य: ये वाक्य किसी तथ्य या जानकारी को नकारते हैं। उदाहरण: "मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा।"
- प्रश्नवाचक वाक्य: ये वाक्य प्रश्न पूछते हैं। उदाहरण: "क्या तुम कल आओगे?"
- आज्ञावाचक वाक्य: ये वाक्य आज्ञा, आदेश या निर्देश देते हैं। उदाहरण: "कृपया दरवाजा खोलो।"
- विस्मयादिबोधक वाक्य: ये वाक्य आश्चर्य, खुशी, दुख या अन्य भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उदाहरण: "वाह! कितना सुंदर दृश्य है!"
- इच्छावाचक वाक्य: ये वाक्य इच्छा, कामना या आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। उदाहरण: "भगवान करे तुम सफल हो।"
- संदेहवाचक वाक्य: ये वाक्य संदेह या संभावना व्यक्त करते हैं। उदाहरण: "शायद आज बारिश होगी।"
- रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार:
- सरल वाक्य: इन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उदाहरण: "राम खेलता है।"
- संयुक्त वाक्य: ये वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बने होते हैं, जो संयोजक शब्दों (जैसे और, या, लेकिन) से जुड़े होते हैं। उदाहरण: "राम खेलता है और श्याम पढ़ता है।"
- मिश्रित वाक्य: इन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। उदाहरण: "जब बारिश होगी, तब हम घर जाएंगे।"
- प्रयोग के आधार पर वाक्य के प्रकार:
- कर्तृवाच्य वाक्य: इन वाक्यों में कर्ता प्रमुख होता है। उदाहरण: "राम ने रोटी खाई।"
- कर्मवाच्य वाक्य: इन वाक्यों में कर्म प्रमुख होता है। उदाहरण: "रोटी राम के द्वारा खाई गई।"
- भाववाच्य वाक्य: इन वाक्यों में क्रिया का भाव प्रमुख होता है। उदाहरण: "मुझसे चला नहीं जाता।"
समास
- समास का अर्थ है संक्षेप में करना।
- जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, तो उसे समास कहते हैं।
- समास के प्रकार:
- अव्ययीभाव समास: इस समास में पहला पद अव्यय होता है और वह प्रधान होता है। उदाहरण: "यथाशक्ति" (शक्ति के अनुसार)।
- तत्पुरुष समास: इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद के कारक चिह्न का लोप हो जाता है। उदाहरण: "राजकुमार" (राजा का कुमार)।
- कर्मधारय समास: इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। उदाहरण: "नीलकमल" (नीला कमल)।
- द्विगु समास: इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। उदाहरण: "त्रिकोण" (तीन कोणों का समूह)।
- द्वंद्व समास: इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और "और" या "अथवा" का लोप हो जाता है। उदाहरण: "माता-पिता" (माता और पिता)।
- बहुव्रीहि समास: इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि एक नया अर्थ निकलता है। उदाहरण: "लंबोदर" (लंबा है उदर जिसका - गणेश)।
संधि
- संधि का अर्थ है मेल या जोड़।
- जब दो वर्ण (स्वर या व्यंजन) आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं।
- संधि के प्रकार:
- स्वर संधि: जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, तो स्वर संधि होती है। स्वर संधि के पांच प्रकार हैं:
- दीर्घ संधि: जब दो समान स्वर मिलते हैं, तो वे दीर्घ हो जाते हैं। उदाहरण: "अ + अ = आ" (विद्या + अर्थी = विद्यार्थी)।
- गुण संधि: जब "अ" या "आ" के बाद "इ", "ई", "उ", "ऊ" या "ऋ" आते हैं, तो वे क्रमशः "ए", "ओ" और "अर्" में बदल जाते हैं। उदाहरण: "अ + इ = ए" (सुर + इंद्र = सुरेंद्र)।
- वृद्धि संधि: जब "अ" या "आ" के बाद "ए", "ऐ", "ओ" या "औ" आते हैं, तो वे क्रमशः "ऐ" और "औ" में बदल जाते हैं। उदाहरण: "अ + ए = ऐ" (एक + एक = एकैक)।
- यण संधि: जब "इ", "ई", "उ", "ऊ" या "ऋ" के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो वे क्रमशः "य्", "व्" और "र्" में बदल जाते हैं। उदाहरण: "इ + अ = य" (यदि + अपि = यद्यपि)।
- अयादि संधि: जब "ए", "ऐ", "ओ" या "औ" के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो वे क्रमशः "अय", "आय", "अव" और "आव" में बदल जाते हैं। उदाहरण: "ए + अ = अय" (ने + अन = नयन)।
- व्यंजन संधि: जब एक व्यंजन का मेल दूसरे व्यंजन या स्वर से होता है, तो व्यंजन संधि होती है। उदाहरण: "उत् + लास = उल्लास"।
- विसर्ग संधि: जब विसर्ग (:) का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, तो विसर्ग संधि होती है। उदाहरण: "निः + चल = निश्चल"।
- स्वर संधि: जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, तो स्वर संधि होती है। स्वर संधि के पांच प्रकार हैं:
वचन
- वचन का अर्थ है संख्या।
- व्याकरण में, वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के उन रूपों को कहते हैं जिनसे उनकी संख्या का बोध होता है।
- वचन के प्रकार:
- एकवचन: जब किसी शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो उसे एकवचन कहते हैं। उदाहरण: "लड़का", "पुस्तक"।
- बहुवचन: जब किसी शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, तो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण: "लड़के", "पुस्तकें"।
- वचन परिवर्तन के नियम:
- आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में "एँ" लगाने से बहुवचन बनता है। उदाहरण: "लता - लताएँ"।
- इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में "याँ" लगाने से बहुवचन बनता है। उदाहरण: "नदी - नदियाँ", "देवी - देवियाँ"।
- उकारांत और ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में "एँ" लगाने से बहुवचन बनता है। उदाहरण: "वधू - वधूएँ"।
- कुछ शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण: "पानी", "आग"।
- कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। उदाहरण: "प्राण", "दर्शन"।
विराम चिह्न
- विराम चिह्न वे चिह्न होते हैं जिनका प्रयोग लिखते समय वाक्यों को अलग-अलग भागों में विभाजित करने और उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है।
- कुछ प्रमुख विराम चिह्न:
- पूर्ण विराम (।): यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है।
- अल्प विराम (,): यह वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए लगाया जाता है।
- अर्ध विराम (;) : यह अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए लगाया जाता है।
- प्रश्नवाचक चिह्न (?): यह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है।
- विस्मयादिबोधक चिह्न (!): यह आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है।
- योजक चिह्न (-): यह दो शब्दों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है।
- निर्देशक चिह्न (—): यह वाक्य में किसी बात को स्पष्ट करने या उदाहरण देने के लिए लगाया जाता है।
- उद्धरण चिह्न (“ ”): यह किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए लगाया जाता है।
- कोष्ठक चिह्न (()): यह वाक्य में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए लगाया जाता है।
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.